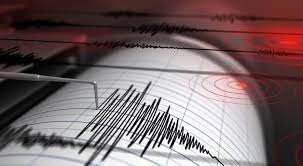DMT : केरला : (12 मई 2023) : –
क्या आज की तारीख़ में सिनेमा समाज में प्रोपेगैंडा का एक हथियार बन गया है? हाल ही में आई फ़िल्म ‘द केरला स्टोरी’ के रिलीज़ होने के बाद ये बहस दोबारा छिड़ गई है, इससे पहले ऐसा कश्मीर फ़ाइल्स के रिलीज़ के समय हुआ था.
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका ये बयान ख़ूब वायरल हुआ.
उन्होंने कहा, “कहते हैं कि केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीति पर आधारित है. देश का एक राज्य जहाँ के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस ‘द केरला स्टोरी’ फ़िल्म में किया गया है.”
विपक्ष के कई नेताओं का कहना था कि “इस्लाम-विरोधी प्रचार” कुछ फ़िल्मों का मुख्य नैरेटिव बन गया है जिसका “राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश” सत्ताधारी पार्टी कर रही है.
पश्चिम बंगाल ने फ़िल्म पर बैन लगा दिया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. कुछ राज्यों ने इसे अपने यहां टैक्स फ्री करने का भी एलान किया है. कुछ जगहों पर फिल्म की स्क्रीनिंग राजनेताओं के लिए भी की गई है.
फ़िल्मों के प्रोपेगैंडा का हथियार बनने के आरोप पर प्रोफ़ेसर इरा भास्कर कहती हैं, “अब कई फ़िल्में सिर्फ़ बहुसंख्यकों की बात करती हैं. केरला स्टोरी मैंने देखी नहीं है लेकिन जितना उसके बारे में पढ़ा यही लगता है कि वो इस्लाम के खिल़ाफ़ ख़ौफ़ पैदा करने के लिए बनी है.”
वे कहती हैं, “कश्मीर पर पहले भी फ़िल्में बनी हैं-‘मिशन कश्मीर’, लम्हा जिसमें भारत, पाकिस्तान सबकी आलोचना है.”
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सिनेमा के बारे में पढ़ाने वाली प्रोफ़ेसर भास्कर कहती हैं, “ये वो फ़िल्में थीं जो सत्ता के खिलाफ़ आवाज़ उठाती थीं लेकिन वो फ़िल्में इस्लामोफोबिक फ़िल्में नहीं हैं.”
“वो दिखाती थीं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, न हिंदुओं के साथ, न मुसलमानों के साथ, लेकिन आज के राजनीतिक हालात में सिनेमा को प्रोपेगैंडा का हथियार बना लिया गया है. इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश हो रही है, चाहे किताबें हों या फ़िल्में.”
वहीं ‘द केरला स्टोरी’ के निर्माता विपुल शाह प्रोपेगैंडा के आरोप पर फ़िल्म के आँकड़ों और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी ढाल बनाते हुए कहते हैं, “जवाब लोगों ने दे दिया है . शुक्रवार के मुकाबले सोमवार को फ़िल्म ने और भी ज़्यादा कमाई की है.”
निर्माता विपुल शाह कहते हैं, “हमारी फ़िल्म किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है. हमारी फ़िल्म आतंकवाद के ख़िलाफ़ है.”
विपुल शाह सवाल उठाने वालों पर आरोप लगाते हैं, “ये सवाल बार-बार पूछकर आप भड़का रहे हैं. हम शुक्रगुज़ार हैं जेपी नड्डा ने हमारी फ़िल्म देखी और तारीफ़ की.”
“ये कहना बेवकूफ़ी वाली बात होगी, कि चूंकि उन्होंने फ़िल्म देखी है इससे साबित होता है कि हम बीजेपी के प्रोपेगैंडा वाली फ़िल्म बना रहे हैं.”
क्या कोई नई बात है?
प्रोपेगैंडा की बहस को समझने के लिए अतीत में झाँकना ज़रूरी है. किस्सा 1975 के आस-पास का है जब भारत में इमरजेंसी का दौर था. ये वो वक़्त भी था जब अभिनेता मनोज कुमार अपनी ख़ास तरह की फ़िल्मों की वजह से ‘भारत कुमार’ के तौर पर पहचान बना चुके थे.
मनोज कुमार इंदिरा गांधी के लिए ‘नया भारत’ नाम की फ़िल्म बना रहे थे लेकिन फिर इमरजेंसी को लेकर आलोचना बहुत बढ़ गई और मनोज कुमार ने फ़िल्म बनाने से इनकार कर दिया.
इसके बाद मनोज कुमार की आने वाली फ़िल्म ‘शोर’ रिलीज़ से पहले ही दूरदर्शन पर दिखा दी गई जिससे थिएटर में रिलीज़ होने पर फ़िल्म के कारोबार पर बुरा असर पड़ा.
इतना ही नहीं, उनकी एक और फ़िल्म ‘दस नंबरी’ के रिलीज़ में भी दिक़्क़त हुई.
अगर इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की पसंद की फ़िल्म बनी होती तो वो प्रोपगैंडा फ़िल्म होती या नहीं, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है.
सिनेमा बना राजनीति की ढाल?
अभी तो बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या राजनेता ‘द केरला स्टोरी’, ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’ जैसी फ़िल्मों का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा के लिए करते हैं या ये कि कई फ़िल्मकार जान-बूझकर प्रोपगैंडा वाली फ़िल्में बनाते हैं,
प्रोपेगैंडा वाली बहस के बीच ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’ के रिलीज़ के वक़्त लेखक राहुल पंडिता ने बीबीसी से बात की थी.
उनका कहना था, “कश्मीर फ़ाइल्स फ़िल्म को इतनी ज़ोरदार सफलता मिली क्योंकि कश्मीरी पंडितों को लगता रहा है कि उनकी कहानी को हमेशा दबाया गया है.”
राहुल ने कहा, “मेरी किताब को छपे 10 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी मेरे पास रोज़ लोगों के ईमेल आते हैं कि उन्हें इस त्रासदी के स्तर का अंदाज़ा ही नहीं था.”
कश्मीर पर दो चर्चित किताबें लिख चुके अशोक कुमार पांडेय का कहना है, “कश्मीरी पंडितों की तकलीफ़ से कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन कश्मीर फ़ाइल्स एक इकहरी फ़िल्म थी जिसमें यह बात पूरी तरह से गोल कर दी गई कि घाटी के मुसलमान भी आतंकवाद से प्रभावित हुए थे.”
“दरअसल, आतंकवाद के दौर में घाटी में मारे गए कुल लोगों में अधिक तादाद मुसलमानों की थी लेकिन फ़िल्म का मक़सद कश्मीर के दर्द को दिखाना कम, और हिंदुओं के पीड़ित होने की भावना को उभारना अधिक था.”
बहरहाल, सत्ता पक्ष से जुड़े अनेक लोगों ने जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे, ‘कश्मीर फ़ाइल्स’ को पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित बताया था.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फ़िल्म के कलाकारों को बधाई दी थी. यह भी दिलचस्प है कि जैसे इस वक़्त ‘द केरला स्टोरी’ को कई भाजपा शासित राज्यों ने टैक्स-फ्री कर दिया है.
प्रोफ़ेसर इरा भास्कर कहती हैं कि नेहरू और दूसरी पार्टियों के शासनकाल में भी विचारधारा से जुड़ी फ़िल्में बनी हैं लेकिन वो क्रिटिकल फ़िल्में कही जा सकती हैं.
मसलन, कुछ साल पहले जब मनोज कुमार सेहतमंद थे तो उन्होंने बीबीसी से ख़ास बातचीत की थी. उन्होंने बताया था कि ‘उपकार’ फ़िल्म की प्रेरणा उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिली थी.
लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री आवास पर निमंत्रित करके कहा था कि क्या वो ‘जय जवान-जय किसान’ की अवधारणा के इर्द-गिर्द फ़िल्म बना सकते हैं.
1950 और 60 का दौर नेहरू का था जब देश में उनका कद बहुत ऊँचा था और उनकी नीतियों और आदर्शों की छाप राज कपूर या दिलीप कुमार और दूसरों की फ़िल्मों पर देखी जा सकती थी.
वहीं जब फ़िल्म जागृति (1954) में स्कूल का टीचर बच्चों को ‘हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल के’ सुनाता है तो बीच गाने में कैमरा नेहरू की फ़ोटो पर ज़ूम होता है और बोल हैं, ‘देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा’.
हम हिंदुस्तानी (1960) में सुनील दत्त पर फ़िल्माया गाना ‘छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी’. इस गाने में भी आप नेहरू को किसी सम्मेलन में देख सकते हैं जो कांग्रेस का अधिवेशन लगता है.
सॉफ़्ट प्रोपेगैंडा बनाम उग्र प्रचार?
तो सवाल उठता है कि क्या ये आदर्शों से प्रभावित फ़िल्में थीं या ये भी एक तरह का सॉफ़्ट प्रोपेगैंडा था और अब ‘द केरला स्टोरी’ में जो हो रहा है वो उसी का बड़ा और उग्र रूप है?
इरा भास्कर अपनी बात कुछ यूँ रखती हैं, “पहले की फ़िल्में किसी समुदाय के खिलाफ़ नहीं होती थीं, वो विकास से जुड़ी हुई या समुदायों को जोड़ने वाली फ़िल्में थीं. दिलीप कुमार की ‘नया दौर’ ऐसी ही फ़िल्म थी जिसमें विकास की बात थी.”
मेघनाद देसाई ने तो इस पर एक किताब भी लिखी है नेहरूज़ हीरो- दिलीप कुमार इन द लाइफ़ ऑफ़ इंडिया.
वो लिखते हैं, “दिलीप कुमार की ‘नया दौर’ नेहरूवियन फ़िल्म थी. फ़िल्म दिखाती है कि लोगों में देश को लेकर एक तरह का गौरव का भाव था, जब वो गाते हैं, ‘ये देश है वीर जवानों का’. इसमें जैसे तांगे और मोटर गाड़ी का टकराव है, वो नेहरू के दौर में आधुनिकीकरण और गांधी की सोच को दर्शाता है.”
आज के दौर की बात करें तो जब 2022 में विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्म ‘कश्मीर फ़ाइल्स’ रिलीज़ हुई जिसने समाज को दो फाड़ कर दिया.
कश्मीर फ़ाइल्स एक यूनिवर्सिटी छात्र की काल्पनिक कहानी है जिसे पता चलता है कि उसके कश्मीरी हिंदू माता-पिता की हत्या इस्लामिक चरमपंथियों ने की थी.
मोदी के भाषण में केरला स्टोरी का ज़िक्र क्यों?
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में फ़िल्म का ज़िक्र करते हुए कहा था, “कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है उस सत्य को सालों तक दबाने का प्रयास किया गया. कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं. आपने देखा होगा, इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया.”
“कई सत्य को दबाने का लगातार प्रयास किया गया. जब हमने भारत विभाजन के दिन 14 अगस्त को हॉरर डे के रूप में याद करने का फ़ैसला लिया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई. कैसे भूल सकता है देश. क्या भारत विभाजन पर कोई ऑथेंटिक फ़िल्म बनी?”
इससे पहले विवेक अग्निहोत्री द ‘ताशकंद फ़ाइल्स’ की भी इस बात की आलोचना हुई थी कि उसमें अफ़वाहों को तथ्य के तौर पर दिखाया गया जिसके बाद शास्त्री के पोते ने क़ानूनी नोटिस भेजा.
सवाल ये भी उठ रहा है कि एक प्रधानमंत्री का बार-बार यूँ विवादित फ़िल्मों का उल्लेख करना कहाँ तक सही है.
‘द केरला स्टोरी’ के ट्रेलर को लेकर ही विवाद हो गया था जब ये दिखाया गया था, “केरल की 32 हज़ार महिलाएँ जिहाद में शामिल हो गई हैं”.
जब अदालत ने फ़िल्म के निर्माता से पूछा कि 32 हज़ार का आँकड़ा कहाँ से आया, तो वो जिसे अब तक ‘तथ्य’ बता रहे थे, उसका ज़िक्र ट्रेलर से हटाने को राज़ी हो गए.
फ़िल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी कहते हैं, “इन फ़िल्मों के निर्माता-निर्देशकों का दावा है कि ये फ़िल्में सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन ये घटनाएँ ज़्यादा पहले की नहीं हैं इसलिए कई बातें लोगों की जानकारी में हैं जिसकी पुष्टि वो खुद कर सकते हैं.”
वे कहते हैं, “कोई भी ये समझ सकता है कि फिल्ममेकर्स का मकसद आम आदमी को उकसाकर, उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना है. इसमें दिए गए तथ्य आधे-अधूरे हैं और विषय-वस्तु को जान-बूझकर भगवा रंग देने की कोशिश की गई है.”
“मुसलमानों को खलनायक या समाज में बुराई की एकमात्र जड़ के रूप में दिखाया गया है.”
रौनक कोटेचा दुबई में फ़िल्म समीक्षक हैं जहाँ केरल समुदाय भी बसा हुआ है. वे कहते हैं, “यहाँ बसे भारतीयों का मकसद सिर्फ़ रोज़ी रोटी कमाना और शांति से रहना है.”
“इसलिए. ज़्यादातर लोग यहाँ पर इन सब बातों पर चुप ही रहते हैं. यहाँ के मीडिया में भी आपको ‘द केरला स्टोरी’ पर ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं देगा.”
सिनेमा और राजनीति का उलझा रिश्ता
वैसे सिनेमा और राजनीति का उलझा हुआ नाता रहा है. जहाँ कुछ फ़िल्मों को राजनीतिक प्रोपेगैंडा के हथियार बनाने का आरोप लगा तो कुछ फ़िल्मों ने सत्ता को चुनौती दी.
जब फ़िल्म ‘किस्सा कुर्सी का’ आई तो संजय गांधी पर आरोप था कि इमरजेंसी के दौरान 1975 में बनी फ़िल्म के प्रिंट उनके कहने पर जला दिए गए थे.
इमरजेंसी के बाद बने शाह कमीशन ने संजय गांधी को इस मामले में दोषी पाया था और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया हालांकि बाद में फ़ैसला पलट दिया गया .
फ़िल्म में संजय गांधी और उनके कई करीबियों का मज़ाक बनाया गया था. शबाना आज़मी गूँगी जनता का प्रतीक थी, उत्पल दत्त एक बाबा के रोल में थे और मनोहर सिंह एक राजनेता के रोल में थे जो एक जादुई दवा पीने के बाद अजब-ग़ज़ब फ़ैसले लेने लगते हैं.
इसी तरह 1978 में आईएस जौहर की फ़िल्म ‘नसबंदी’ भी संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रम का मज़ाक उड़ाती थी जिसमें उस दौर के बड़े सितारों के डुप्लिकेट ने काम किया था. फ़िल्म में दिखाया गया कि किस तरह से नसबंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया.
फ़िल्म का एक गाना था ‘गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार’ जिसके बोल कुछ यूँ थे, “कितने ही निर्दोष यहाँ मीसा के अंदर बंद हुए/अपनी सत्ता रखने को जो छीने जनता के अधिकार/गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार”
इसे इत्तेफ़ाक़ कहिए या सोचा-समझा क़दम कि ये गाना किशोर कुमार ने गाया था. दरअसल, इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार उस वक़्त बहुत नाराज़ हो गए थे जब उन्हें कांग्रेस की रैली में गाने के लिए कहा गया.
प्रीतिश नंदी के साथ छपे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, “मैं किसी के आदेश पर नहीं गाता.”
जब इमरजेंसी के दौरान कलाकारों ने उठाई आवाज़
किशोर कुमार और देव आनंद ने जिस तरह इमरजेंसी का विरोध किया इसके किस्से तो जगज़ाहिर हैं.
देव आनंद तो इतने नाराज़ थे कि उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम की राजनीतिक पार्टी तक बनाई थी. शिवाजी पार्क में इसका बड़ा जलसा भी हुआ.
सिनेमा, कांग्रेस, भाजपा, लेफ़्ट, प्रोपेगैंडा ..ये तार उलझे हुए लगते हैं लेकिन इसमें कई अपवाद भी रहे हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने सिनेमा प्रेम के लिए जाने जाते रहे हैं. फ़िल्म ‘कोई मिल गया’ की ख़ास स्क्रीनिंग राकेश रोशन ने वाजपेयी के लिए रखी थी लेकिन उस वक़्त कोई विवाद नहीं हुआ था.
इतना ही नहीं, आमिर खान ने अपनी फ़िल्म ‘तारे ज़मीं पर’ (2007) की ख़ास स्क्रीनिंग लालकृष्ण आडवाणी के लिए रखी थी जिसके बाद ये सुर्खी मशहूर हुई थी कि फ़िल्म ने फ़िल्म क्रिटिक रहे आडवाणी को रुला दिया था.
जबकि इससे पहले 2006 में नर्मदा बचाओ आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण आमिर संघ परिवार के निशाने पर थे और आमिर की फ़िल्म ‘फ़ना’ गुजरात में बैन भी कर दी गई थी.
प्रोपैगैंडा बनाम मनोरंजन
पिछले कई सालों से भारत में ऐसी फ़िल्में बन रही हैं जो देश में लोकप्रिय मुद्दों और सरकार की नीतियों के अनुरूप कहानियाँ चुन रही हैं.
स्वच्छ भारत को देखते हुए ‘टॉयलेट एक प्रेमकथा’ और उद्यम को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को ध्यान में रखकर बनी ‘सुई-धागा’ सरकारी योजनाओं के प्रचार पर आधारित लगती हैं.
देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के दौर में ऐसी ऐतिहासिक फ़िल्मों की बाढ़ आ गई है जिनमें हिंदू सेनानियों की वीरता और ‘मुसलमान आक्रांताओं’ की क्रूरता को दिखाया जा रहा है, जैसा कि फ़िल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी ने भी कहा. तानाजी, पृथ्वीराज, पद्मावत, पानीपत और बाजीराव मस्तानी वग़ैरह ऐसी फ़िल्में हैं.
धर्म, समुदाय, दंगों और जातीय हिंसा को लेकर भी फ़िल्में बनती रही हैं. पंजाब के हालात को लेकर 90 के दशक में गुलज़ार ने ‘माचिस’ बनाई. राहुल ढोलकिया की ‘परज़ानिया’ आई.
पंजाब में दंगों पर ‘पंजाब 1984’ आई. बँटवारे से पहले हुई धार्मिक हिंसा पर ‘तमस’ जैसी टेलीफ़िल्म बनी. ‘गर्म हवा’ में बँटवारे के बाद का दर्द दिखाया गया.
1959 में जब यश चोपड़ा ने अपनी पहली फ़िल्म निर्देशित की तो एक ऐसे मुसलमान व्यक्ति पर बनाई जो एक नाजायज़ हिंदू बच्चे को गोद लेता है और दो साल बाद ही वो ‘धर्मपुत्र’ बनाते हैं जो बँटवारे के बाद एक हिंदू युवक, उसकी धार्मिक कट्टरता और बदलाव की कहानी है.
इन पर प्रोपेगैंडा के आरोप नहीं लगे, लेकिन आज के बँटे हुए समाज में ये अंतर धूमिल-सा होता दिखता है कि किस फ़िल्म में समाज की सच्चाईयों को दिखाने की कोशिश की गई है, कहाँ केवल कोरा प्रोपेगैंडा है.
जैसा कि कश्मीर फ़ाइल्स से जुड़ी एक बातचीत में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकर सिद्धार्थ काक ने कहा था , “कश्मीर फ़ाइल्स को लेकर कहा गया कि यही सच है. लेकिन कश्मीरी पंडितों की कहानी आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप पिछले 30 सालों के कश्मीर की कहानी न बताई जाए.”
“शायद यही वजह है कि फ़िल्मों में इनकी कहानी पहले नहीं दिखाई गई क्योंकि इन जटिल मुद्दों को जिस तरह परत-दर-परत दिखाने की ज़रूरत है, उसे कहने का शायद स्पेस ही नहीं है.”
अंत में ज़िक्र मनोज कुमार का, उन्होंने राज्यसभा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, “मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है लेकिन मैं इंसान दरबारी नहीं हूँ. मैं किसी नेता के ड्राइंग रूम में बैठने वाला नहीं हूँ. मेरी नेता मेरी पब्लिक है.”